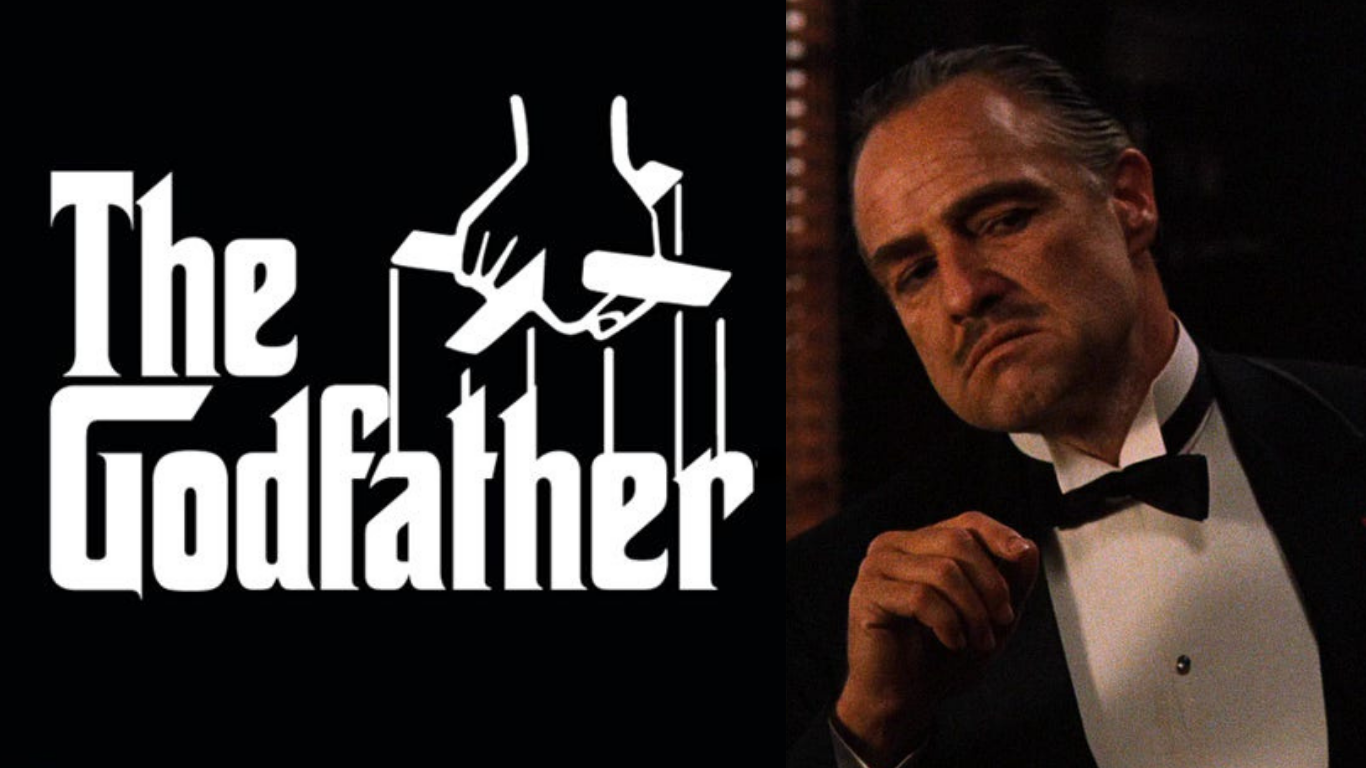कल्पना कीजिए आपको पता चले कि आपकी माँ किसी से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? बहुत से लोगों के लिए तो इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल होगा, स्वीकार करना तो दूर की बात है। त्रासदी एक ऐसे ही माँ बेटे की कहानी है। जहाँ माँ एक छोटे से गाँव में रह कर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाह रही है और बेटा अपनी माँ को समाज द्वारा गढ़ी परिभाषित माँ के खाँचे में ढालना चाहता है। नाटक में आप एक माँ के क़िरदार में सच्ची नारीवादी महिला को देखेंगे और बेटे के क़िरदार में आप एक ऐसे मर्द को देखेंगे, जिसको समाज की सोच ने लड़के से तथाकथित मर्द बना दिया है। नाटक में माँ बेटे के संवाद आपको हर बार समाज के विचारों पर सवाल उठाने पर मज़बूर कर देंगे।
नाटक का वो संवाद जहाँ बेटा कोपल कहता है कि “अरे, माएँ कहाँ नास्तिक होती हैं, माँ नास्तिक नहीं होती हैं।” जिसपर वो कहती है “अब मैं तो हूँ” संवाद की यह पंक्ति सीधा आपकी सोच पर प्रहार करती है। आगे के डायलॉग में वो कहती है कि “हम सब इस दुनिया में ज़्यादा नास्तिक हैं कम आस्तिक हैं।” अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती है “देखो इस देश में लगभग दस धर्म होंगे। उसमें से नौ तो तू नहीं मानता है, बस एक मानता है न। तो उन नौ धर्मों के लिए हम दोनों साथ में नास्तिक हुए न। मैं तो बस एक और धर्म नहीं मानती।” इसी संवाद में आगे एक डायलॉग आता है जो धर्म कैसे पितृसत्ता से जुड़ा है दर्शकों को समझाने की कोशिश करता है- “हर धर्म में मुख्य भूमिका तो पुरुषों की ही है… तो वो तो मानेंगे। हम औरतों का तो हर धर्म में सपोर्टिग रोल है… तो मैं तो नहीं मानूँगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि औरतें क्यों इसे स्वीकार करती हैं? मैं नहीं करुंगी, मेरा अब सपोर्टिंग रोल नहीं है। मेरे जीवन में मेरी भूमिका मुख्य है।” माँ के क़िरदार द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ उसकी तार्किक नारीवादी सोच को दर्शकों के सामने रखती है।
कोपल ‘मेरे जीवन में मेरी भूमिका मुख्य है’ वाली बात पर माँ से पूछ बैठता है कि और मैं? मैं कहा हूँ आपके जीवन में? जिसपर माँ का जवाब सुन आपको इन्सान होने का सही अर्थ समझ आएगा- “तुम अहम क़िरदार हो। मुख्य तो कोई नहीं है, मैं मेरे जीवन में मुख्य हूँ, जैसे तुम्हारे जीवन में तुम।”
और पढ़ें: शीला दावरे: ऑटो रिक्शा की स्टेयरिंग संभालकर समाज की सोच बदलने वाली महिला
नाटक के हर संवाद में माँ का नारीवादी व्यक्तित्व आपको दिखेगा। जब भले ही बेटे ने माँ को स्लीवलेस ब्लॉउज़ पहनने से रोकना हो या बेटे के जाने के बाद अपने प्यार के साथ एक घर में रहना हो। माँ की नारीवादी सोच से परेशान हो कोपल माँ को गाँव से मुम्बई ले जाने के लिए कहता है- “‘माँ क्या रखा है इस गाँव में, यहाँ वैसे भी लोग अजीब-अजीब बातें करते हैं। बंबई ग़ज़ब शहर है। चलो माँ अब से हम दोनों वहीं रहेंगे। वहाँ आपको जैसे रहना हो आप रहना, जो करना है वो करना, खुली छूट है आपको।” जिसपर माँ कहती है- “तू बंबई जा तेरे को वहाँ जैसे रहना है रह, जो करना है कर, खुली छूट हो तेरे को, मैं तो यहाँ वैसे ही रह रही हूँ जैसा मुझे रहना है।” कोपल मनाने के इरादे से कहता है “माँ कभी तो मेरी बात सुनो… लोग क्या कहेंगे कि जैसे ही मुझे बंबई में जॉब मिली मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर भाग गया।” इस पर दूसरी तरफ से समाज को चाटा मारता हुआ जवाब आता है “तो उन लोगों को कहना कि तेरी माँ विकलांग नहीं है, उसके हाथ पैर सही चलते हैं, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है।” ये डायलॉग दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि महिला को हमेशा किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। वो खुद भी अपना ख़्याल रख सकती है। वो अपनी ज़िन्दगी अपनी शर्तों पर जी सकती है।
नाटक में आगे जहाँ माँ और बेटे के बीच में माँ के प्रेमी को ले कर एक संवाद होता है जिसमें वो दर्शकों और बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि एक महिला को समाज में सभ्य बनने के लिए समाज के बनाए गए अलग-अलग रोल में रहना पड़ता है। महिला की अपनी खुद की पहचान इसमें कई गुम हो जाती है। वो एक इन्सान की तरह ज़िन्दगी नहीं जी पाती है- “अच्छी बेटी की, अच्छी माँ की, अच्छी बीवी की, अच्छी औरत की, अच्छी टीचर की… जाने कितनी दुकानें खोल रखी थीं। मैं कब से लोगों को वही बेच रही थी जो लोग ख़रीदना चाहते थे। पर लोगों की अपेक्षाएँ ख़त्म नहीं होती, मैं इस उम्र में और कितनी दुकानें खोलूँ? इस सब में मैं क्या चाहती हूँ मेरे पास उसकी कोई जगह ही नहीं बची थी, उसकी एक टपरी तक नहीं थी मेरे पास। सो मैंने बहुत पहले अपनी सारी दुकानों के शटर गिरा दिए हैं। मैं अब किसी को कुछ नहीं बेच रही हूँ। न लोगों को और न ही तुझे।” माँ का क़िरदार नारीवादी होने का सही अर्थ हर बार लोगों के सामने रखता है।
और देखें: Angry Young Men: सलीम-जावेद, हिन्दी सिनेमा में पटकथा लेखन के चमकते सितारे
तो वहीं दूसरी तरफ बेटे का क़िरदार उम्र के अलग अलग पड़ाव में बदलाव से गुज़रता है। बचपन में खुद को पेड़ का पत्ता तो अपनी माँ को पेड़ मानना हो या फिर थोड़ा बड़े होने के बाद उसी माँ के नास्तिक होने और माँ की ज़िन्दगी का मुख्य क़िरदार न होने से समस्या होना क्यों न हो। बचपन में उसकी बातों में जहाँ बचपना दिखता है तो वहीं उम्र के दूसरे पड़ाव में मर्दों जैसी बातें करता दिखता है। नाटक में जब उसको माँ से मिलने आने वाले लोगों से और स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनने से आपत्ति होती है। तब वो दर्शकों को कहता है-“मैंने देखा था, इसके बाद भी माँ ने अपने जीने में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं किए। वो जैसी थी वैसी की वैसी रहीं।” फिर कोपल माँ से मूक युद्ध करता है जहाँ वो दर्शकों को बताता है “फिर एक दिन माँ पूरी बाँह का ब्लाउज़ पहनकर स्कूल जा रही हैं। मैं तुरंत घर भागा और उनके सारे स्लीवलेस ब्लाउज़ उठाए और घर से दूर जाकर एक कूड़ेदान में फेंक दिए। पर आप आश्चर्य करेंगे इससे मेरी माँ को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा। घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। माँ हर कुछ दिनों में एक नया स्लीवलेस का ब्लाउज़ सिलवा लाती और मैं, जब भी मौक़ा मिलता उस ब्लाउज़ को कूड़े दान में फेंक आता।” ये दृश्य लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक बच्चा जिसने उम्र के दूसरे पड़ाव में क़दम रखा है और उसकी सोच पर अभी से पितृसत्ता ने पकड़ बना ली है। इस संवाद से पहले कोपल अपने पक्के दोस्त सुधीर से माँ को ले कर संवाद भी करता दिखता है। ये संवाद बच्चों की बातों में कैसे पितृसत्ता घर करती है, दर्शकों को समझाने का प्रयास करती है।
इसके साथ ही एक सटल तरीके इस बात पर भी गौर करवाती है कि कैसे एक मां के साथ पलने बढ़ने वाला बच्चा भी समाज से सारी दुनिया की बातें सीख रहा है। चूंकि अगर उसने मां से सीखा होता तो शायद मां की तरह सा सोचता विचारता। लेकिन उसने अपने आस पास के लोगों और अपने समाज के लोगों से सीखा है।
जब कोपल मुम्बई जॉब कर रहा होता है और सुधीर के बताने पर कि माँ अब किसी गैरमर्द के साथ रह रही है तो वो माँ से बिना बात करे तुरन्त वापस गाँव आता है और अपनी बदनामी न हो इसके लिए माँ को मुम्बई ले जाना चाहता है। नाटक का ये खण्ड आपको ये बताना चाहता है कि समाज के लिए महिला का सभ्य ही बना रहना सही है वरना इसमें महिला की बदनामी नहीं होती है इससे उस घर की और उस घर के मर्दों की बदनामी होती है।
कोपल अंत में कहता है कि “इस जलती हुई लकड़ी को पकड़े हुए मैं एक सैनिक लग रहा था जिसका काम था मरने तक अपनी माँ पर पहरा देना। मैं वही हो गया था… कठोर। कितना कठोर था मैं। मैं कोपल नहीं था।” वो अंत आते आते ये भी मानता है कि वो इस पितृसत्तात्मक समाज का शिकार हो गया है। वो अपनी माँ के लिए अपने बाप की तरह बन गया था जो माँ को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। कोपल का बाप कभी भी माँ को लिखने नहीं देता था। घर के सारे पेन तोड़ देता था ताकि उसकी माँ लिख न सके। घर से बाहर जाते हुए वो कोपल की माँ को घर में बंद कर के जाता है। वो कभी भी अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहता था। पर समाज ने उसको उसके बाप की तरह बना दिया था।
कोपल के क़िरदार में निरंतर बदलाव दिखता है। नाटक के शुरुआत में कोपल अपनी माँ को गोर्की की माँ पलाग्या निलोवना से तुलना करता दिखता है। तो अंत में वो कहता है कि “मेरी माँ पेलाग्या निलोवना थी, मैं ही गोर्की नहीं हो पाया था।” अगर आप नाटक देखेंगे या फिर उस नाटक को जब पढ़ेंगे तब आपको कोपल शुरू में माँ को अधिकतम बार ‘मेरी माँ’ बोलता दिखेगा, जो अंत आते आते केवल ‘माँ’ हो जाती है। ये परिवर्तन दर्शा रहा है कि कैसे कोपल पहले माँ को अपनी प्रॉपर्टी मानता था पर अंत में वो उसको केवल माँ के रूप में देख रहा है। उसका अलग अस्तित्व स्वीकार रहा है। वो उसके लिए अब प्रॉपर्टी नहीं रही अब वो एक इन्सान है जो अपनी शर्तों पर अपनी ज़िन्दगी जी सकती है।
यहाँ पर नाटक पढ़ें: त्रास्दी (नाटक) Solo play…. Manav Kaul Traasadi