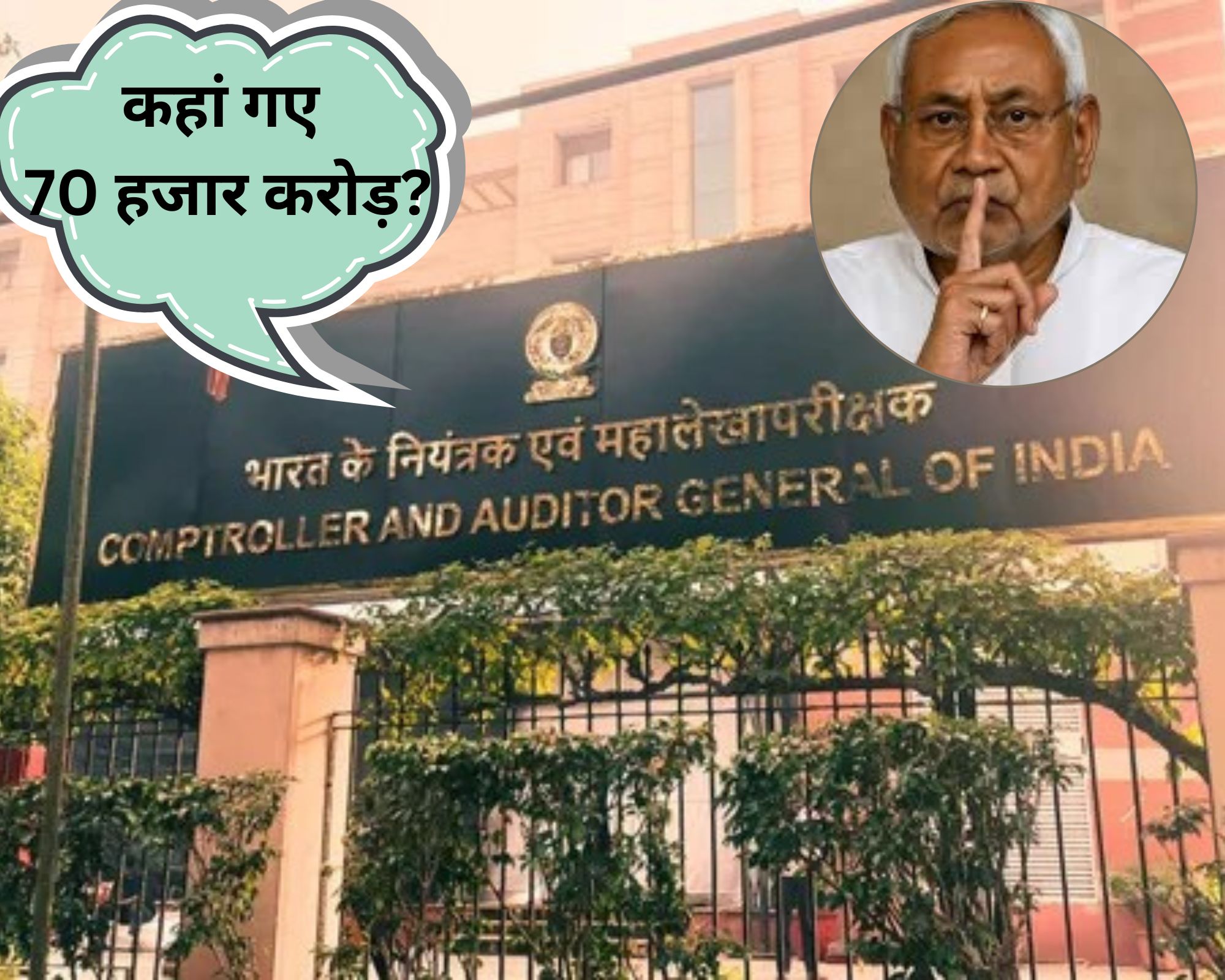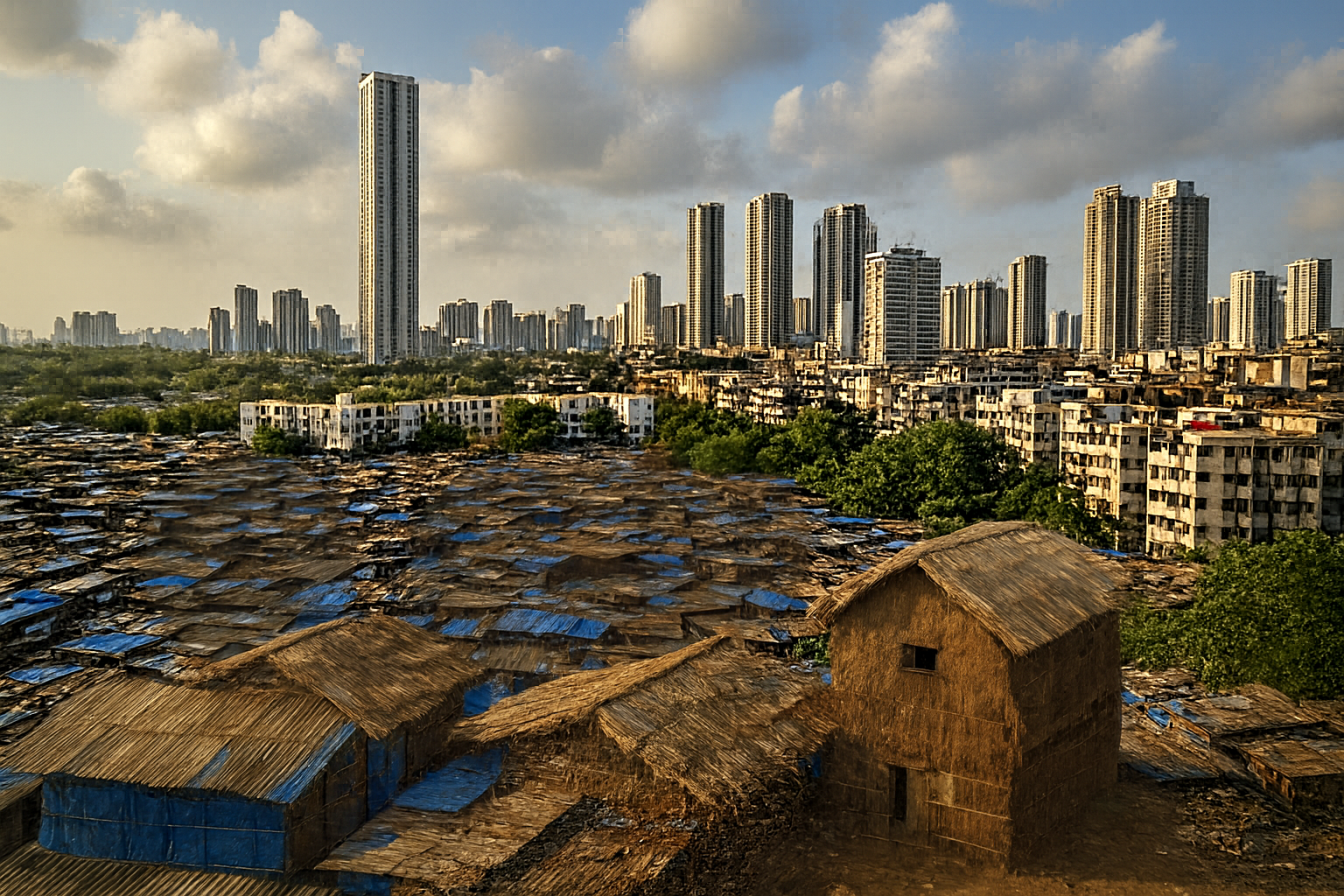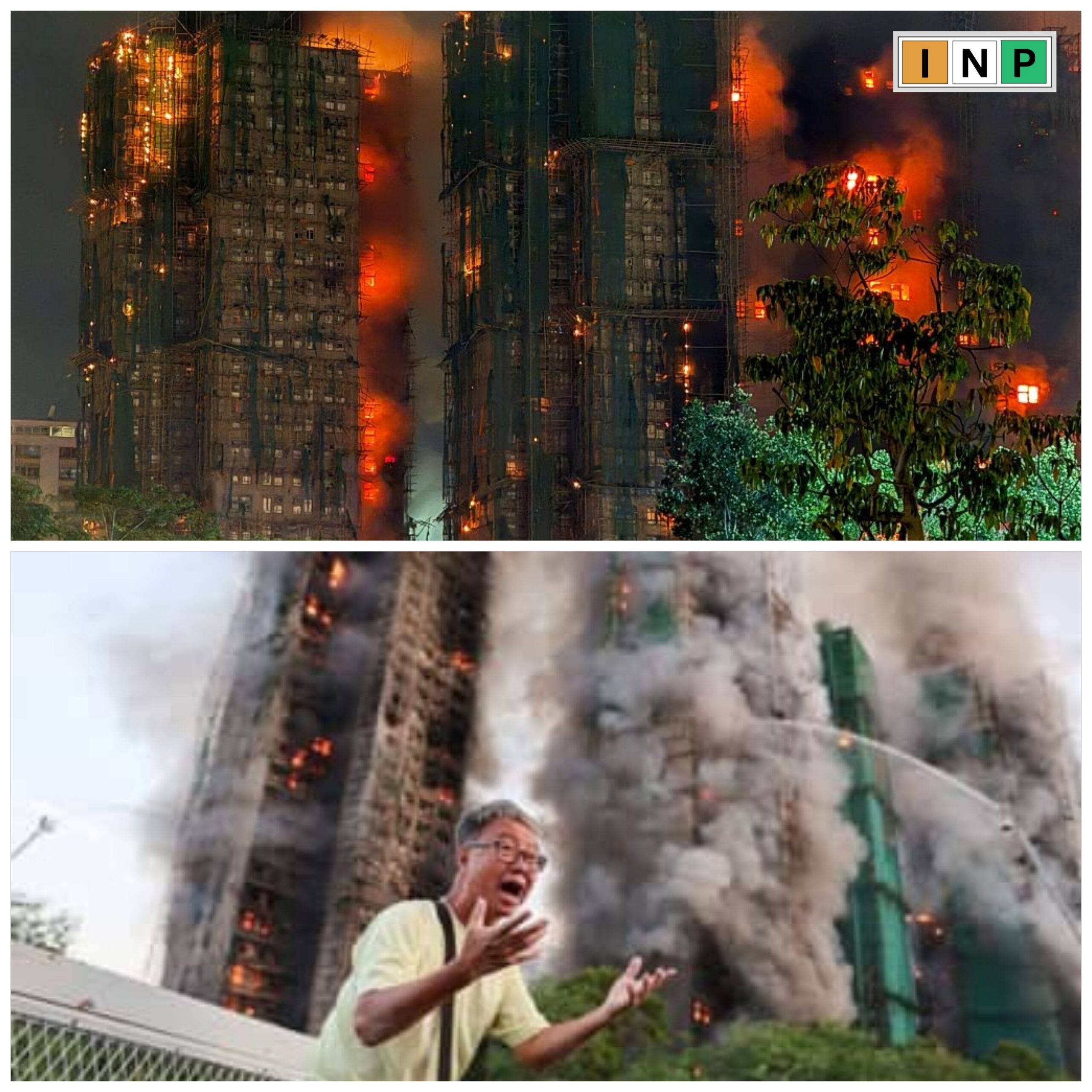इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राज्य की राजनीति में हलचल तेज़ होती जा रही है। राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय। हर पार्टी अपनी रणनीति के पत्ते खोलने में लगी है। एक ओर चुनाव आयोग मतदाता सूची के पुनः सत्यापन और पहचान पत्रों की जांच में जुटा है, तो दूसरी ओर जनता की निगाहें मौजूदा सरकार पर टिकी हैं, जिसने सत्ता में एक लंबी पारी खेली है। सवाल यह है कि क्या इस बार शिक्षा का मुद्दा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा पाएगा?
बिहार, जिसकी पहचान प्राचीन भारत में शिक्षा और ज्ञान के केंद्र के रूप में रही है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की गौरवगाथा आज भी दुनिया में मिसाल मानी जाती है। लेकिन मौजूदा तस्वीर इस गौरवशाली विरासत से जरा भी मेल नहीं खाती। आज का बिहार अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जूझ रहा है। यह संघर्ष हर चुनाव में नई घोषणाओं और वादों के साथ दोहराया जाता है।
चुनाव से पहले योजनाओं और घोषणाओं की बाढ़ आना आम बात है। इस बार भी वही हो रहा है। मौजूदा सरकार शिक्षा क्षेत्र में नई घोषणाओं और पुराने वादों के दोहराव से जनता को साधने की कोशिश कर रही है। विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा बता रहा है। जनता के मन में सवाल है, क्या यह घोषणाएं सिर्फ वोट हासिल करने का साधन हैं या वास्तव में शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम देने की मंशा है?
शुरुआती सुधार और बदलाव की नींव
नीतीश कुमार की पहली सरकार (2005-2010) को शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल के लिए याद किया जाता है। उस दौर में मिड-डे मील योजना और खासकर साइकिल योजना ने गांव-गांव में शिक्षा का परिदृश्य बदला।
पहले जहां गरीब परिवार बेटियों को यह कहकर स्कूल नहीं भेजते थे कि घर और खेत का काम कौन करेगा, वहीं साइकिल और स्कूल ड्रेस ने सोच बदली। अचानक हजारों-लाखों बच्चियों का नाम स्कूलों में दर्ज होने लगा। यह सामाजिक बदलाव मामूली नहीं था। पहली बार लड़कियों ने बड़ी संख्या में स्कूल की दहलीज पार की और हाथ में कलम थामी।
इसी दौरान जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत हुई और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शुरू हुई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) लागू होने के बाद सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया। हालांकि चुनौतियां तब भी थीं और आज भी बरकरार हैं।
शिक्षा और रोजगार का सीधा रिश्ता
बिहार में शिक्षा केवल बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला नहीं, बल्कि यह रोजगार का बड़ा साधन भी है। 2009-10 में जहां राज्य में 2.66 लाख सरकारी शिक्षक थे, वहीं मार्च 2025 तक यह संख्या बढ़कर 5.80 लाख से अधिक हो गई। यह दिखाता है कि शिक्षा क्षेत्र ने न केवल विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया बल्कि रोजगार भी बड़े पैमाने पर पैदा किया।
हाल ही में मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं जिसमें आने वाली शिक्षक भर्तियों में 35% महिला आरक्षण और डोमिसाइल नीति लागू होगी। लंबे समय से यह मांग उठती रही थी कि बिहार की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले। इस फैसले से जहां राज्य के बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सकती है, वहीं यह चुनावी समीकरण को भी साधने की कोशिश मानी जा रही है।
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा: खोई हुई कड़ी
बावजूद इसके, सवाल यही है कि क्या नियुक्तियों से शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ी है? ग्रामीण इलाकों में अब भी कई स्कूल भवन का इंतजार कर रहे हैं। कई जगह बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। कहीं जर्जर दीवारों के सहारे कक्षाएं चलती हैं। बारिश होते ही कक्षा पांच तक के बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। बढ़ती जनसंख्या और सीमित स्कूल क्षमता ने हालात और बिगाड़ दिए हैं।
कमजोर बच्चों को अतिरिक्त एक घंटा पढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया था। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां मौसम अत्यधिक गर्म और ठंडा होता है, यह प्रयोग असफल साबित हुआ। कई बच्चों की जान चली गई। भारी विरोध के बाद यह आदेश वापस लेना पड़ा। सवाल उठता है, क्या शिक्षा सुधार के नाम पर बिना सोच-विचार किए प्रयोग किए जा रहे हैं?
नियुक्ति और विवादों की राजनीति
बिहार में शिक्षा की बहस बिना TET परीक्षाओं और शिक्षक नियुक्ति विवादों के अधूरी है। पिछले एक दशक में बार-बार ऐसी परीक्षाएं हुईं जिन पर कोर्ट की रोक लगी। फाइलें वर्षों तक अटकी रहीं और अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ा। हर चुनाव से पहले सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का एलान करती है, लेकिन अमल की रफ्तार पर सवाल उठते हैं।
यही कारण है कि हजारों अभ्यर्थी आज भी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और यह मुद्दा चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बन गया है।
लाइब्रेरी और लैब की भारी कमी
जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें विज्ञान और तकनीक से जुड़े प्रयोगशालाओं और लाइब्रेरियों की जरूरत होती है। लेकिन बिहार के अधिकांश सरकारी स्कूल आज भी इन सुविधाओं से वंचित हैं। कंप्यूटर लैब तो नाम मात्र के हैं। ग्रामीण इलाकों में तो बच्चे कंप्यूटर को सिर्फ किताबों में तस्वीरों के रूप में देखते हैं।
जबकि दुनिया डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ रही है, बिहार के बच्चे आधारभूत संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। यह अंतर चुनावी बहस का हिस्सा बनना ही चाहिए।
उच्च शिक्षा की दुर्दशा
साइकिल योजना ने लड़कियों को स्कूल तक तो पहुंचाया, लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।
विश्वविद्यालयों का हाल यह है कि तीन साल का कोर्स पांच से छह साल में पूरा होता है। परीक्षाएं सालों-साल लटकती रहती हैं। कई छात्र अंततः इग्नू या दूसरे शहरों के कॉलेजों में दाखिला लेने को मजबूर होते हैं। यह स्थिति न केवल छात्रों का समय बर्बाद करती है बल्कि उनके आत्मविश्वास और करियर को भी नुकसान पहुंचाती है।
ड्रॉप आउट बना सबसे बड़ा संकट
- यूडीआईएसई-प्लस की ताजा रिपोर्ट (2022-23 से 2023-24) बिहार के लिए खतरे की घंटी है।
- 20.86% छात्र स्कूल छोड़ देते हैं—यह देश में सबसे अधिक है।
- प्राथमिक स्तर पर GER 41.9% से घटकर 41.5%।
- मध्य स्तर पर 96.9% से गिरकर 96.5%।
- माध्यमिक स्तर पर 90% से गिरकर 89.5%।
लड़कों की तुलना में लड़कियों की ड्रॉपआउट दर माध्यमिक स्तर पर थोड़ी ज्यादा है। इसके पीछे गरीबी, ढांचागत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता प्रमुख कारण बताए जाते हैं।
शिक्षा और जीवन कौशल का तालमेल
बिहार, जहां की 68 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, उनके बच्चे खेतों और प्रकृति से जुड़े रहते हैं। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने उन्हें जमीन से काटना शुरू कर दिया है।
बड़े निजी स्कूलों में बच्चे पॉटरी बनाना, बागवानी करना और खेती-किसानी सीखते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा प्रोजेक्टर और स्लाइड शो तक सीमित है। किताबों और टैबलेट तक सीमित शिक्षा बच्चों को जीवन कौशल से वंचित कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना ही असली सुधार होगा।
चुनावी मौसम और शिक्षा का एजेंडा
चुनावी साल में शिक्षा का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। सरकार शिक्षकों की भर्ती, नई नीतियों और भवन निर्माण की घोषणाओं को अपनी उपलब्धि बताती है। विपक्ष इसे चुनावी जुमला करार देता है।
राजद का कहना है कि अगर सरकार गंभीर होती तो उच्च शिक्षा की दुर्दशा इतनी भयावह न होती। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी लगातार शिक्षा बजट घटाने का मुद्दा उठाती रही हैं।
क्या है आगे की राह
- नए स्कूल भवन – बढ़ती जनसंख्या के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाना।
- विश्वविद्यालय सुधार – सेशन डिले खत्म करना और शोध कार्यों को बढ़ावा देना।
- शिक्षक प्रशिक्षण – शिक्षकों को पढ़ाई पर केंद्रित करना, उन्हें क्लेरिकल कामों से दूर रखना।
- लाइब्रेरी और लैब – हर स्कूल में आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था।
- समाज की भागीदारी – संपन्न लोग जमीन और संसाधन दान कर शिक्षा सुधार में सहयोग दें।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक ओर गौरवशाली अतीत है, दूसरी ओर वर्तमान की चुनौतियां। चुनावी मौसम में यह मुद्दा भले ही चर्चा में है, लेकिन असली सवाल यही है—क्या आने वाली सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठा पाएगी? शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। अगर सरकार और समाज मिलकर काम करें, तो नालंदा और विक्रमशिला की धरती एक बार फिर से ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बन सकती है।