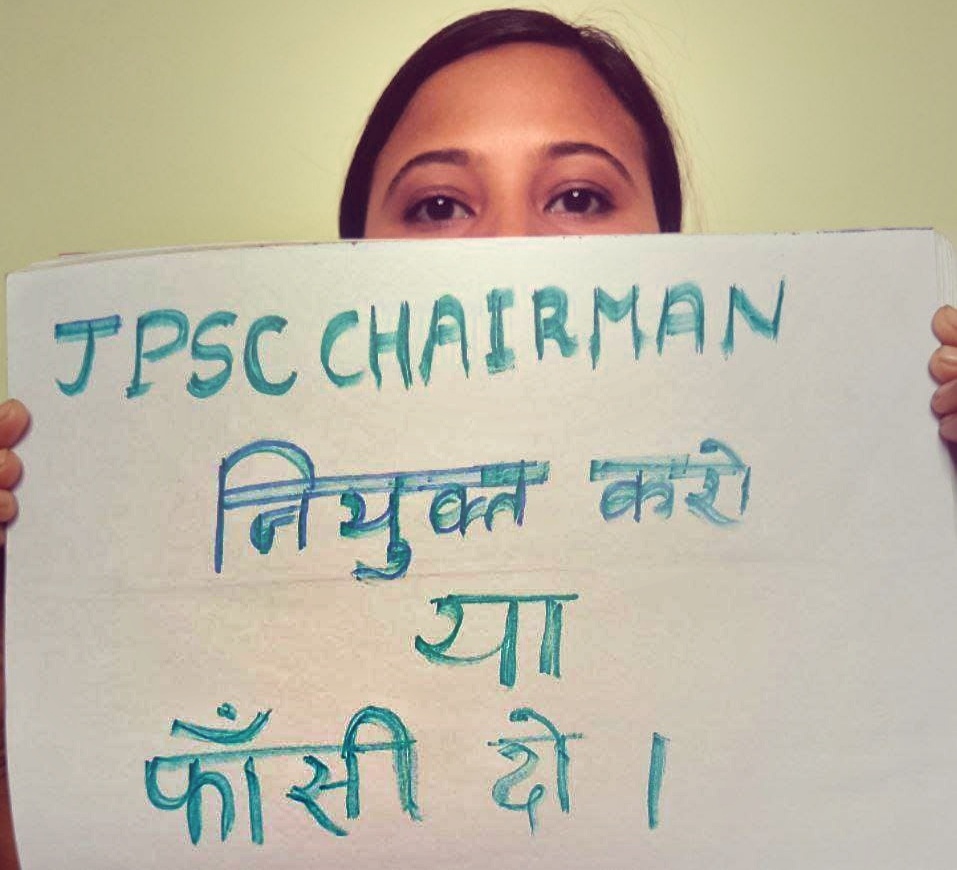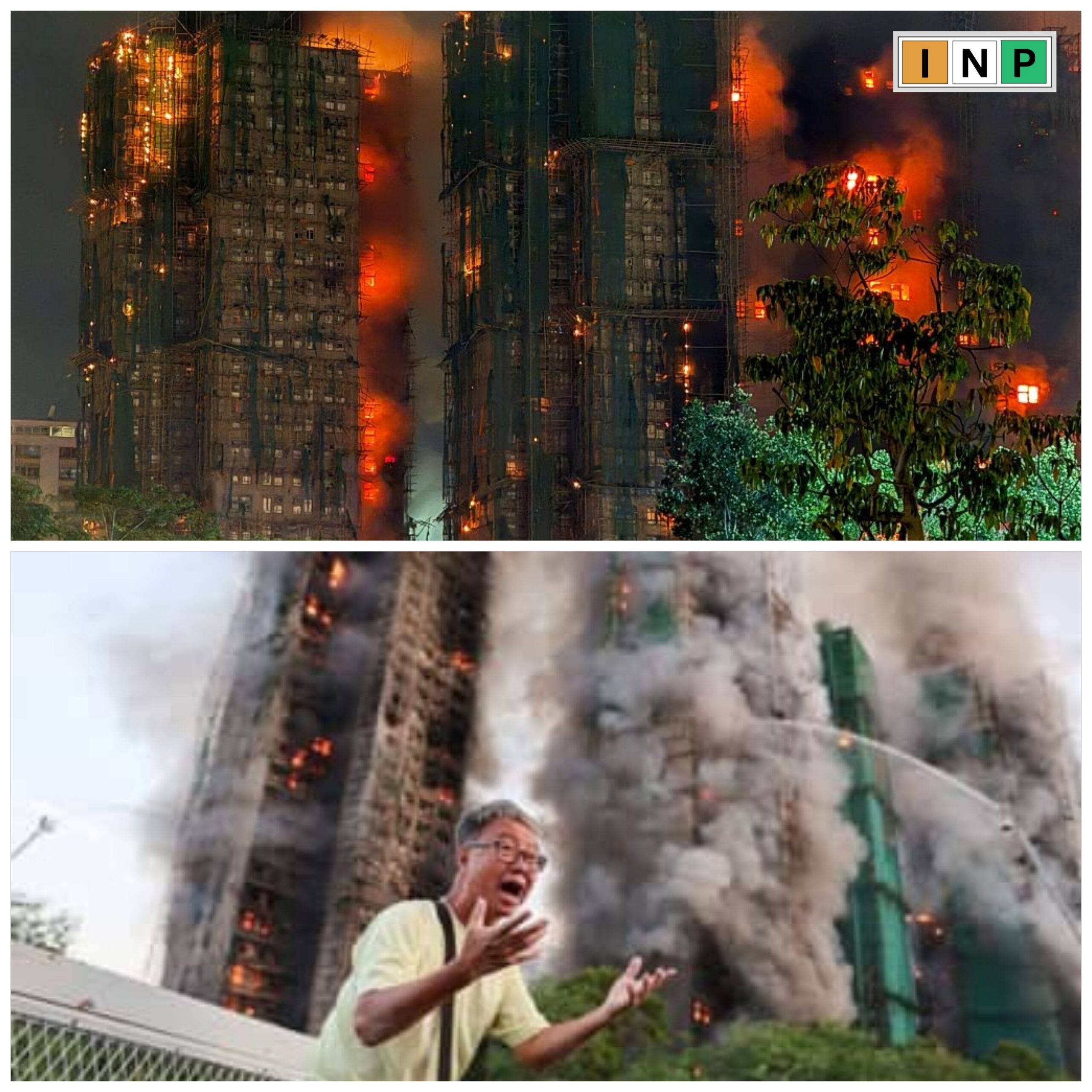“क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या आदिवासी होना ही हमारा गुनाह है? क्या हम सरकारी योजनाओं के लायक नहीं हैं? सरकारें आ रहीं, जा रहीं। लेकिन हमारा जीवन वहीं का वहीं है।” ये शब्द हैं एक जनजातीय शख्स के, जो बिहार के एक आदिवासी गांव में रहता है। मगर ये कहानी 30 परिवार के करीब 250 लोगों की है, जो जमुई जिला से महज 45 किलोमीटर दूर बामदह पंचायत के पिपरा सरायसोल गांव में रहते हैं। इस गांव में आजादी के 78 साल बाद भी बेसिक जरूरत कही जाने वाली आम सुविधाएं जैसे साफ पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य नहीं पहुंचा है। आधी-अधूरी मात्रा में अगर कोई योजना गई भी है, तो या तो वो अटकी पड़ी है या फिर खस्ता हालत में गांव वालों को चिढ़ाती हुई सरकार की नाकामी दिखा रही है।
आइए हम आपको ले चलते गांव की ऊबड़-खाबड़ सैर पर, जहां आपको कदम-कदम पर हर वो चुनौती देखने को मिलेगी जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में शायद ही झेलते हों।
नदी में चुआं खोदकर बुझाते हैं प्यास
गांव की बड़की मरांडी बताती हैं कि इस गांव के 250 लोगों की प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा है यह नदी का चुआं। सर्दी, गर्मी या बरसात, चुआं के पानी पर ही गांव की पूरी आबादी निर्भर है। नदी तक पानी लाने के लिए ग्रामीणों को एक किलोमीटर तक पथरीले रास्तों पर चलना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष अपने सिर पर हांडी में पानी भरकर लाते हैं। मरांडी बताती हैं कि गांव के छोटे-छोटे बच्चे गर्मियों में यह काम करते हैं, शाम तक नदी में सभी बच्चे मिलकर कई गड्ढे खोद देते हैं, तब जाकर अगली सुबह हम लोगों की प्यास बुझती है। यह संघर्ष सालों से सुबह से शुरू होकर शाम तक ऐसे ही चलता रहता है।
वहीं गांव के नयका मरांडी और सोमरा मुर्मू कहते हैं कि साहब गर्मियों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। हमें कहीं भी पानी जल्दी नहीं मिलता है। गांव के पुरुष और कामकाजी महिलाएं भी दिनभर जहां-तहां जोरिया में चुआं खोदकर पानी निकालने के लिए भटकते रहते हैं। इतना कहते ही उनका गला भर आया है और भावुक होकर कहते हैं कि साहब! ‘हम आदिवासी हैं, इसलिए हमें पानी तक के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है।’
मूंह बिरबाता चापाकल और कुआं
गांव में 250 की आबादी पर केवल एक चापाकल और एक ही कुआं है। इसने भी सरकार की तरह यहां काम करना बंद कर दिया है। पूरे दिन में महज तीन-चार बाल्टी पानी निकालने वाला नल लोगों को चिढ़ाता हुआ सरकारी तंत्र की सच्चाई बयां करता हुआ नजर आता है। कुआं में कचड़ा जमने से धीरे-धीरे जल स्त्रोत कम हो गया है। चापाकल खराब है, पानी नहीं आता है। गांव वालों ने बताया कि मुखिया को कई बार लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन हमारी समस्याएं जस की तस रहीं। मिलता है तो बस आश्वासन। सरकार की नल जल योजना का लाभ कागजों तक ही सीमित रह गया है।
सरकारी पानी की योजनाओं के कागजी दावे
गांव में पानी की असलियत आप जान गए। अब पढ़िए, सरकार के बड़े-बड़े दावे, जो मगज कागजों और पुरस्कारों तक सीमित हो गए हैं। सरकार कहती है कि बिहार के 70-80 फीसदी घरों तक नल जल योजना पहुंच चुकी है, लेकिन जिले के तमाम प्रखंडों की स्थिति कुछ और ही असलियत बयां करती हैं।
अप्रैल 2023 में बिहार-झारखंड सीमा पर स्थित जमुई जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अर्धवार्षिक जल जीवन सर्वेक्षण-2023 (जेजेएस) में जमुई जिला को पुरस्कार मिला था। जिले को ‘हाई अचीवर्स’ की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला था। इसका मतलब यह है कि इसने 75-100 प्रतिशत जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल कनेक्शन हासिल कर लिया है। जमुई जिला 100 प्रतिशत कनेक्शन वाले जिलों की श्रेणी ‘फ्रंटरनर्स’ के बाद दूसरे स्थान पर था।
राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने 6 जुलाई को पुरस्कार के बारे में इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था। जेजेएस रैंकिंग 55 लीटर से अधिक पानी प्रति व्यक्ति, प्रति दिन प्राप्त करने वाले घरों का प्रतिशत, पोर्टेबिलिटी और नियमितता पैरामीटर, स्रोत स्थिरता, क्लोरीनीकरण, उपयोगकर्ता शुल्क और शिकायत निवारण प्रणाली जैसे संकेतकों पर आधारित था।
राज्य की राजधानी पटना में पीएचईडी विभाग के मुख्य अभियंता सह विशेष सचिव अशोक कुमार ने कहा, “जमुई आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आता है – जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों द्वारा परिभाषित हैं। इसके बावजूद, इसने जेजेएस में अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए, जमुई को यह पुरस्कार मिला। हालांकि, अगर हम बिहार के अन्य जिलों से तुलना करें, तो इस संबंध में जिले के सभी पत्रकार एक ही सुर में कहते हैं कि किसी भी प्रखंड के किसी भी पंचायत में एचजीएनजेवाई योजना के तहत 50 प्रतिशत तक भी काम नहीं हुआ है।
HGNJY बिहार की अपनी योजना है, जो केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन (JJM) से अलग है। इसे 27 सितंबर, 2016 को लॉन्च किया गया था और इसमें दिन में तीन बार दो-दो घंटे पानी की आपूर्ति का वादा किया गया था। HGNJY का लक्ष्य मार्च 2020 तक पूरे राज्य में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना था। 2021 तक, बिहार के HGNJY ने JJM के तहत 8.44 लाख कनेक्शन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से 2.32 लाख कनेक्शन की तुलना में 152.16 लाख नल कनेक्शन हासिल किए थे। पीएचईडी के अधिकारियों की मानें तो दो लाख घरों को अभी भी कनेक्शन का इंतजार है। पिपरा सरायसोल के ये 30 आदिवासी परिवार भी उन्हीं घरों में से एक हैं, जहां आज भी पानी नहीं पहुंचा है। ना ही केंद्र सरकार की मदद से और ना ही राज्य सरकार की मदद से।
हाली-बीमारी में इंतजार और दूरियों का दंश झेलते आदिवासी
गांव में न तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और न ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बीमार होने पर ग्रामीणों को 20 किलोमीटर दूर चकाई बाजार जाना पड़ता है। स्थिति इतनी खराब है कि रात के समय कोई बड़ी समस्या हो तो गांव के लोग भगवान भरोसे जीते हैं। उनके पास अपनी मौत और सुबह होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि इस आदिवासी गांव में रात के समय कोई स्थानीय डाक्टर भी जंगली क्षेत्र होने के कारण आने-जाने से कतराता है।
साल भर से बिजली गुल, अंधेरे में डूबा गांव
गांव के लोग पिछले एक साल से बिना बिजली के घुप अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। गांव में बिजली तो पहुंची है, मगर खराब ट्रांसफार्मर के चलते गांव रोशनी को मोहताज है। गांव के गणेश मुर्मू कहते हैं, “बड़े लोगों का ट्रांसफार्मर खराब हो तो तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन हम जैसे पहाड़ी और आदिवासी लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती।”
रोटी और मकान की हालत भी गंभीर
पिपरा सरायसोल के लोगों को राशन लेने के लिए 9 किलोमीटर दूर बामदह जाना पड़ता है। रास्ता पथरीले और कच्चे रास्तों से होकर जाता है, जिसे खराब मौसम और भी भयानक बना देता है। ये आदिवासी लोग सरकारी आवास योजना के लिए आज भी तरस रहे हैं। इसलिए गांव के ज्यादातर घर आज भी मिट्टी के बने हुए हैं।
रोजगार की कमी से पलायन बना मजबूरी
गांव के पुरुष और महिलाएं पत्तल, दातवन और लकड़ी बेचकर जीवन-यापन करते हैं। गांव वालों की आमदनी का मुख्य स्त्रोत आज भी जंगल ही है। जंगल से गांव के लोगों की गुजर-बसर होती है। मनरेगा जैसी योजना यहां ठंडी पड़ी हुई है। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन मनरेगा यहां निष्क्रिय है। इसलिए बड़े होते जा रहे बच्चे अब रोजगार की तलाश में बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली जैसे अन्य बड़े शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं।
गांव में नहीं है कोई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र
पिपरा सरायसोल गांव में अब तक कोई भी आंगनबाड़ी या सरकारी स्कूल नहीं है। अभी हाल ही में आई यूडायस प्लस 2023-24 की रिपोर्ट में पता चला कि बिहार में ऐसे भी गांव है, जहां एक भी छात्र स्कूल में नहीं है लेकिन शिक्षक नियुक्त हैं। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 117 स्कूल ऐसे हैं जहां की 544 शिक्षक कार्यरत हैं जबकि विद्यालयों में बच्चे एक भी नहीं है। यह रिपोर्ट बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं बड़ी खामियों को दिखाता है। बिहार सरकार अब भी जिले की सुदूर गांव या इलाकों में स्कूल आंगनबाड़ी सुविधाएं बहाल करने में नाकामयाब साबित हो रही हैं।
सड़क निर्माण शुरू, पर अधर में लटकने का डर
हालांकि, गांव में सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ है। यह ग्रामीणों के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन डर है कि कहीं वन विभाग के अड़ंगे के कारण यह काम अधूरा न रह जाए। सड़क का बनना यहां के जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन इस उम्मीद पर अभी भी संशय बना हुआ है।
मोबाइल नेटवर्क के लिए पहाड़ों की चढ़ाई
आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क हर किसी की पहुंच में है, वहीं पिपरा सरायसोल गांव के लोग मोबाइल नेटवर्क के लिए पहाड़ों और टीलों पर चढ़ाई करते हैं। जब किसी से बात करनी होती है तो सिग्नल मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।
इस आदिवासी गांव की यह स्थिति सवाल खड़ा करती है कि क्या वास्तव में भारत गांवों का देश है? क्या महात्मा गांधी ने इसे ही कहा था कि भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। क्या गांधी यही ग्रामीण स्वराज और ग्राम विकास को भारत के विकास का आधार मानते थे। यह दृश्य न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दिखाता है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि विकास के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यह गांव भारत के अनेकों गांवों की सच्ची कहानियां बयां करता है, जो आज भी विकास की राह देख रहे हैं।
इस लेख को लिखने में हमारी मदद जमुई जिला के चंद्रमंडी निवासी, अमित कुमार राय ने की है।
ये लेख भी पढ़ें
झारखंड में नहीं थम रही मानव तस्करी, एक साल में बढ़े 37 फीसदी मामले; जानिए कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित

साल 2007 में झारखंड की बंधनी कुसमा की 12 वर्षीय बेटी मानव तस्करी का शिकार हुई, तो परिवार में विपत्तियों की बाढ़ आ गई। पहले रिश्तेदार के घर से बेटी की किडनैपिंग फिर पति की मौत, इसके बाद पुलिस द्वारा बेटी के अपहरण की शिकायत भी ना दर्ज करना। इस तरह करीब 17 साल तक बंधनी अपनी बेटी को पाने की चाहत में पल-पल घुटती रहीं। पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट।